
‘बाटुइ’ लगाता है पहाड़, भाग—11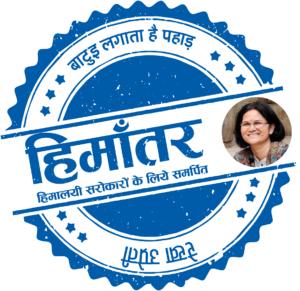
- रेखा उप्रेती
शुरू जाड़ों के दिन थे वे. बर्फ अभी दूर-दूर पहाड़ियों में भी गिरी नहीं थी, पर हवा में बहती सिहरन हमें छू कर बता गयी थी कि खाँकर जम गया होगा… इस्कूल की आधी छुट्टी में पाँचवीं कक्षा में पढ़ने वाले सीनियर्स ने प्रस्ताव रखा “हिटो, खाँकर खाने चलते हैं…” तो आठ-दस बच्चों की टोली चल पड़ी खाँकर की तलाश में…
इस्कूल हमारा पहाड़ के सबसे ऊँचे शिखर पर था और खाँकर मिलता था एकदम नीचे तलहटी पर बहते गधेरे में… वह भी देवदार के घने झुरमुट की उस छाँव के तले, जहाँ सूरज की किरणों का प्रवेश जाड़ों में तो निषिद्ध ही होता…
अपनी पहाड़ी से कूदते-फाँदते नीचे उतर आए हम….उसके लिए हमें बनी-बनाई पगडंडियों की भी ज़रुरत नहीं थी. सीढ़ीदार खेतों से ‘फाव मारकर’ हम धड़धड़ाते हुए उतर आते थे. गाँव की ओर जाने वाली पगडंडी पहले ही छोड़ दी, कोई देख ले तो खाँकर का ख़्वाब धरा रह जाए…… तलहटी पहुँचकर गधेरा मिला तो उसकी धार के विपरीत दिशा में चलने लगे हम. पहाड़ी गधेरों में पानी ज्यादा नहीं होता. सिर्फ बरसातों में आस-पास की पहाड़ियों से बहकर आते ‘रौल-मौल’ के कारण जरूर उनमें बहाव रहता है. जाड़ों में तो बांज के जंगलों से फूटते स्रोतों के पानी से ही सदानीरा रहते हैं गधेरे, तो धार विरल ही रहती है. हाँ, पानी बहुत ठंडा था उन दिनों… पैर डाल दो तो मुरदार हो जाएँ…

गधेरे के दोनों तरफ़ जंगल थे. चीड़, देवदार, बाँज, बुरांश और काफल के घने फैले जंगल.. गाय बछियों के घर लौटने का समय था यह… दरअसल हमारे गाँव के लोग सुबह-सुबह अपने ‘छान’ से गाय-बैल व बड़े बछड़ों को जंगल में ‘हका’ आते थे. आधे दिन तक ‘धुर’ में चर कर वे खुद ही वापस लौट आते… यह भी एक विस्मयकारी तथ्य था कि एक छान के सभी वाशिंदे एक साथ टोली बनाकर घर लौटते थे. पता नहीं कौन पहल करता होगा कि बहुत चर लिया अब चलो घर की ओर.. बाकि बिना प्रतिवाद किए उसका अनुसरण करते होंगें… उन्हें घर का रास्ता याद रहता और अपना खूँटा भी. कभी कोई नयी ब्याई गाय ज़रूर बाकी साथियों को छोड़ जल्दी घर पहुँच जाती और रंभाने लगती कि आ गयी हूँ… बाँध दो खूँटे पर….
दोपहर का समय, जंगल में झींगुरों की झिंग-झिंग के अलावा कोई और स्वर नहीं था… गाँव दूर छूट चुका था और घर लौटती गायों का झुण्ड भी… फिर थोड़ी-थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गयी… बीच-बीच में गधेरे का साथ छोड़ना पड़ता हमें.. वह या तो ऊंची छलांग लगा झरने के आकार ले लेता या सघन झाड़ियों की ओट में छुपम-छुपाई खेलने लग जाता…
उसकी ‘म्हांSS’ सुनकर आमा गाली देती- “ भ्योव पड़ ज्यै…” (खाई में गिरे तू) फिर खूँटे से बाँध उसके गले को थपथपाती और हरी घास का गट्ठर डाल देती उसके सामने…

तो इन गाय-बछियों के झुण्ड से बचते-बचाते हमारी टोली आगे बढ़ती रही. दोपहर का समय, जंगल में झींगुरों की झिंग-झिंग के अलावा कोई और स्वर नहीं था… गाँव दूर छूट चुका था और घर लौटती गायों का झुण्ड भी… फिर थोड़ी-थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गयी… बीच-बीच में गधेरे का साथ छोड़ना पड़ता हमें.. वह या तो ऊंची छलांग लगा झरने के आकार ले लेता या सघन झाड़ियों की ओट में छुपम-छुपाई खेलने लग जाता… पानी की कल-कल से हम उसका दामन पकड़े रहे… यह छूट गया तो जंगल में भटकना निश्चित था… और खाँकर भी इसी के पहलू में मिलना था..… सर्द हवा से कान, गाल और नाक की नोक लाल हो गयी हमारी.. पैरों में कभी किल्मोड़ी के काँटे चुभ जाते तो कभी घिंघारू की झाड़ी में फ़रोक के छोर फँस जाते …
“कितनी दूर मिलेगा खाँकर…” किसी ने पूछा…
“बस थोड़ा-सा आगे…वहाँ…” हमारी टोली का नेतृत्व करने वाले लड़के ने इशारा किया..
आप पहाड़ में किसी से पूछें कि फलाँ जगह कितनी दूर है तो यही जवाब मिलता है… चाहे दो-चार किलोमीटर आगे ही क्यों न हो आप का ठिकाना… ‘बहुत दूर है’ कहने वाले कम ही मिलेंगे पहाड़ में… चलते रहो.. ‘माठु-माँठ’ जैसे पहाड़ की ज़िन्दगी चलती है…
आगे बगुड्यार था… बाघ का ‘उड्यार’ यानी गुफा.. दीदियों से सुन रखा था कि वहाँ बाघ रहता है, अब घिग्घी बंधने लगी हमारी.. कहीं सामने आ गया तो हमारा ही हो जाएगा खाँकर… चुपचाप बिना आवाज़, बिना आहट किए चलने लगे हम… वैसे ही दबे पाँव, जैसे बाघ आता था गाँव में, रात को … और कुत्तों, बकरियों, बछड़ों को उठा ले जाता…
देवदार का जंगल शुरू हुआ तो हमारी जान में जान आई. यहीं कहीं मिलेगा खाँकर… हमने सुन रखा था…
गधेरे के किनारे बैठ कुछ देर सुस्ताए हम… घने पेड़ों से घिरी ढलान पर बैठे हुए दूर सामने की पहाड़ी पर टिके अपने स्कूल को देखा हमने.. अरे!! कितनी दूर आ गए हम… रोज स्कूल से हम इस ‘देवदारबणि’ को देखते थे, आज यहाँ से दिखता अपना इस्कूल बहुत भला लग रहा था…
अगला चरण था वह गंतव्य.. जहाँ हमें खाँकर मिलने वाला था.. दो-तीन लड़कों ने कुछ आगे जाकर आवाज़ लगाईं… “याँ छू याँ…”
और हम सबने दौड़ लगा दी…

गधेरे का पानी यहाँ कुछ ठहरा हुआ सा था.. एक छोटी-सी झील नुमा जगह थी यह… और झील के ऊपर जमा हुआ था खाँकर…
एक साथी ने पास में पड़ी देवदार की लकड़ी से इस दर्पण में दरार कर दी… फिर तो कई चमकीली दरारें चटक उठीं… हम भी टूट पड़े उन पर… आखिर इसी के लिए तो इतना सफ़र तय कर आए थे.. वह भी इस्कूल से भागकर…
हमने उसे छू कर देखा… एक दम ठोस और ठंडा.. पारदर्शी ऐसा कि उसके नीचे पानी की सलवटें, तले पर ठहरी कंकड़ियाँ और उनमें पड़ती झिलमिल परछाइयाँ साफ़ दिख रहीं थीं. खुशी से किलक उठे हम.. बाघ का डर भी हमारी कल्पनाओं से कूच कर गया.
एक साथी ने पास में पड़ी देवदार की लकड़ी से इस दर्पण में दरार कर दी… फिर तो कई चमकीली दरारें चटक उठीं… हम भी टूट पड़े उन पर… आखिर इसी के लिए तो इतना सफ़र तय कर आए थे.. वह भी इस्कूल से भागकर…
एक-एक टुकड़ा उठा हमने दाँतों से कटक मारकर खाया उसे… ऐसा ठंडा और कड़क कि आत्मा तक सिहर उठी… ओह!! कैसा अपूर्व अनुभव…
(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं)
